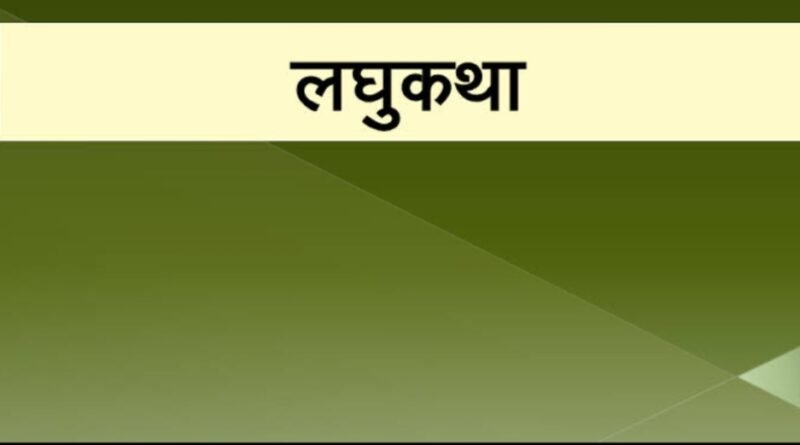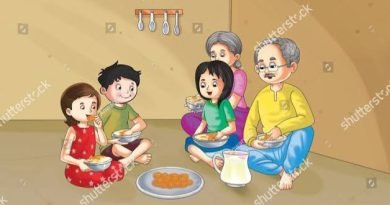प्रियंका सौरभ की लघुकथाएं
21. बर्थडे केक
नीलिमा का जन्मदिन था। सबने बधाइयाँ दीं — पति ने केक मंगाया, बेटे ने गाना गाया। लेकिन नीलिमा की आँखें नम थीं।

कारण? उसे चॉकलेट नहीं, स्ट्रॉबेरी पसंद थी। पर हर साल चॉकलेट ही आता था।
यह छोटी सी बात नहीं थी — यह उसकी पसंद को न समझ पाने का प्रतीक था। शादी के बाद शायद किसी ने पूछा ही नहीं, क्या अच्छा लगता है?
उस रात उसने खुद के लिए एक स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, और उस पर लिखा — “तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा।”
अगले साल परिवार ने पूछा — “क्या केक लाना है?” वह मुस्कुरा दी — “सिर्फ मेरा पसंदीदा, स्ट्रॉबेरी।”
22. गुमनाम विद्रोह
संध्या चुपचाप रहती थी। ऑफिस जाती, काम करती, घर लौटती। सब कहते — “बहुत शांत लड़की है।”
किसी को नहीं पता था, वह हर रात एक डायरी लिखती थी — जिसमें बॉस की तानाशाही, घर की बंदिशें, समाज की अपेक्षाएँ सब दर्ज थीं।
धीरे-धीरे वह डायरी एक किताब बन गई — ‘एक स्त्री की चुप्पियाँ’। उसने गुप्त नाम से पब्लिश करवाई।
किताब बेस्टसेलर बनी, पर लेखक का नाम आज भी ‘गुमनाम’ है।
वह हँसती है — “नाम नहीं चाहिए, पर मेरी आवाज़ अब सिर्फ कागज़ पर नहीं, लोगों के दिल में गूंजती है।”
23. किचन टाइमर
नीरा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था — किचन टाइमर। हर 10 मिनट में ‘टिक टिक’ — कुकर, गैस, मिक्सर, फिर स्कूल की घंटी, फिर पति की चाय।
एक दिन टाइमर ने फिर बजाया और नीरा ने उसे उठाकर खिड़की से फेंक दिया।
बेटा चौंका — “माँ, टाइमर क्यों फेंका?”
नीरा बोली — “आज समय मेरी मर्जी से चलेगा, मशीन की मर्ज़ी से नहीं।”
उसने वो दिन अपने लिए रखा — किताब पढ़ी, चित्र बनाए, पुरानी दोस्त को कॉल किया।
अब नीरा हर सप्ताह एक दिन टाइमर को साइलेंट मोड पर रखती है — और अपने लिए जीती है।
24. लौटती चिट्ठियाँ
अंजू ने शादी के बाद मायके चिट्ठियाँ भेजनी बंद कर दी थीं। सब कहते — “फोन कर लो, क्या ज़रूरत है चिट्ठियों की?”
पर एक दिन पुरानी अलमारी से एक लिफाफा मिला — माँ की चिट्ठी, अधूरी और बिना भेजी गई। उसमें लिखा था — “तू चिट्ठियाँ भेजा कर, पढ़ने से लगता है तू पास है।”
उस दिन अंजू ने फिर से चिट्ठी लिखी — माँ के लिए। जवाब आया — माँ की खुशबू से भीगी चिट्ठी।
अब हर महीने चिट्ठियाँ आती-जाती हैं — कागज़ पर रिश्तों की गर्मी लौटी है।
25. चुप्पियों का मेला
गाँव में सालाना मेला लगा था। सब हँसते, खिलौने खरीदते, झूले झूलते। पर उस मेले में रमा को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया — ‘स्त्रियों की चुप्पियों का पंडाल’।
वह एक कला प्रदर्शनी थी — जहाँ बिंदी, साड़ी, रसोई, चिट्ठियाँ सब प्रतीक बने थे स्त्रियों के भीतर दबी कहानियों के।
रमा देर तक वहाँ खड़ी रही — हर वस्तु जैसे उसकी ज़िंदगी की कोई घटना दोहरा रही थी।
वह लौटकर घर आई, और अपनी बेटी से कहा — “तेरी हर बात सुनी जाएगी, तेरी हर चुप्पी पूछी जाएगी।”
उस दिन से रमा ने घर में एक डायरी रखी — जहाँ सबकी अनकही बातें दर्ज होती हैं। चुप्पियों का मेला अब उसके घर में भी रोज़ लगता है — और हर बार कोई न कोई वहाँ बोल उठता है।
26. परोसने से पहले
संध्या हर रात सबके खाने के बाद ही खाती थी। सब पूछते — “तुम्हें भूख नहीं लगती?” वह मुस्कुरा देती।
पर वह मुस्कुराहट आदत बन चुकी थी, मजबूरी नहीं। वो जानती थी — सबके पसंद का खाना परोसना ही उसका प्यार था।
हर सब्ज़ी, हर रोटी में वह सबके स्वाद, स्वास्थ्य और खुशी को परखती थी। उसके लिए उनका पेट भरना, खुद की आत्मा को तृप्त करने जैसा था। यह उसका रसोईघर नहीं, उसका प्रेमस्थल था।
एक दिन बेटा बोला — “माँ, आज पहले तुम खाओगी, फिर हम।”
संध्या हँसी — “अभी तो चपातियाँ बनानी हैं।”
पर सबने मिलकर कहा — “अब हर रात पहले तुम बैठोगी, हम साथ खाएँगे।”
उस दिन पहली बार संध्या ने बिना परोसे खाना खाया — और पाया, स्वाद में आत्मसम्मान मिला हुआ था। पहली बार उसे लगा कि उसका ‘देना’ देखा और समझा गया।
उस रात उसकी थाली में दाल से अधिक आदर, रोटी से अधिक रिश्ता और सब्ज़ी से अधिक सहानुभूति थी।
27. बिंदी की अलमारी
मीना के पास बिंदियों का एक बॉक्स था — सैकड़ों रंग, आकार, चमक। हर बिंदी उसके किसी खास दिन की गवाह थी।
उसने कभी किसी को नहीं बताया — वह हर दुख के बाद एक नई बिंदी पहनती थी, जैसे जख्म पर रंगीन पट्टी।
पति की नाराज़गी, सास की ताने, दफ्तर की उपेक्षा — हर एक बिंदी उसका प्रतिरोध थी।
कभी गाढ़ी लाल बिंदी किसी संघर्ष की याद दिलाती, तो कभी नीली बिंदी उसके अंदर छिपी ठंडी परत को उजागर करती। कभी वह हँसती बिंदी लगाती, ताकि लोग उसकी आंखों की नमी न देख सकें।
एक दिन बेटी ने पूछा — “माँ, ये इतनी सारी बिंदियाँ क्यों?”
मीना बोली — “ये मेरी चुप लड़ाइयाँ हैं। रंग-बिरंगे हथियार।”
अब बेटी जब भी दुखी होती है, माँ की बिंदी अलमारी से एक बिंदी उठाती है — और साहस पहनती है।
हर सुबह जब मीना बिंदी चुनती है, वह दिन का रंग तय करती है — दुख, हिम्मत, विरोध या सिर्फ खुद की पसंद।
28. शादी का कार्ड
अंजली डाक से आया एक सुनहरा कार्ड देखकर ठिठक गई। ऊपर लिखा था — ‘सौरभ weds राधिका’। वही सौरभ, जिससे उसने कभी सच्चा प्रेम किया था, और जिसने बिना कारण उसे छोड़ दिया था।
वह कार्ड उसके लिए सिर्फ कागज़ नहीं था, वर्षों की प्रतीक्षा, संदेह और अधूरी कविताओं का उत्तर था। उसने कार्ड को उलट-पलटकर देखा — तारीख, स्थान, सब कुछ स्पष्ट था, सिवाय उस दर्द के जो अंजली के भीतर पिघलने लगा।
वह कुछ देर चुप रही, फिर चाय बनाई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। वहाँ से दिखते थे फूलों से लदे पेड़ और खिलते बच्चे — ज़िंदगी का संकेत कि रुकना नहीं है।
उसने कार्ड को फिर देखा और हँसी — “शादी मुबारक हो, सौरभ। तुमने जो अधूरा छोड़ा, वह मैंने खुद पूरा कर लिया है — अपने लिए।”
उसने कार्ड को अलमारी में नहीं, किताबों के बीच नहीं, बल्कि कूड़ेदान में नहीं — अपनी डायरी के पहले पन्ने में रख दिया।
क्योंकि अब वो एक ‘अतीत’ नहीं था, बल्कि उसकी कहानी का एक मजबूत अध्याय बन चुका था। और अंजली जानती थी — अधूरे प्रेम से निकला आत्मसम्मान सबसे मुकम्मल होता है।
29. मोबाइल में छुपा
डर सिमरन का फोन हमेशा लॉक रहता था। किसी को भी पासवर्ड न पता था — न माँ को, न बहन को।
पर उस लॉक के पीछे सिर्फ चैट्स नहीं थीं, एक डर था — किसी के ‘देख लेने’ का।
कॉलेज में सब कहते थे — “तेरा बॉयफ्रेंड कितना पज़ेसिव है! कितना प्यार करता है!”
पर किसी को नहीं पता था कि वह प्यार नहीं, नियंत्रण था। हर कॉल पर हिसाब, हर पोस्ट पर सवाल, हर मैसेज पर शक।
धीरे-धीरे सिमरन ने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुस्कुराना भी कम कर दिया।
एक दिन माँ ने पूछा — “तू खुश है, बिटिया?”
सिमरन चुप रही, पर उसकी आँखें बोल उठीं।
रात को उसने मोबाइल उठाया, वह डर जो उसमें कैद था, उसे मिटाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले वह चैट डिलीट की जिसमें बार-बार तौहीन थी, फिर नंबर ब्लॉक किया।
सुबह उसका फोन अब भी लॉक था, पर अब वह मुस्कुरा रही थी। क्योंकि अब उसमें डर नहीं, साहस छुपा था।
30. खुद से मिलना
नम्रता दो बच्चों की माँ, एक जिम्मेदार बहू, एक सहयोगी पत्नी और एक कुशल गृहिणी थी। लेकिन इन सभी पहचानों में एक नाम कहीं खो गया था — ‘नम्रता’।
हर दिन सुबह पाँच बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, सास-ससुर की दवाइयों का ध्यान रखना, पति के टिफिन में सलाद काटना — दिन पूरा होने से पहले ही खुद का दिन खत्म हो जाता।
एक दिन उसने पुराने अलबम में एक तस्वीर देखी — कॉलेज की पेंटिंग प्रतियोगिता में अवार्ड लेते हुए।
वह तस्वीर जैसे उसके भीतर कहीं सोई कलाकार को जगा गई। उस शाम उसने बच्चों से कहा — “आज डिनर बाहर से मँगवाते हैं।”
सब चौंके, पर मान गए। रात को जब सब सो गए, नम्रता ने पुराने रंग, ब्रश और कैनवास निकाले। बरसों बाद पहली बार उसने कुछ रंगों से बात की।
हर स्ट्रोक के साथ वह खुद के करीब आती गई।
सुबह दीवार पर उसकी बनाई पहली पेंटिंग टंगी थी — और मुस्कुराती नम्रता भी।
कभी-कभी खुद से मिलना ज़रूरी होता है — ताकि हम फिर से सबके लिए बेहतर बन सकें।
31. बर्थडे केक
अदिति हर साल बेटी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाती थी। रंग-बिरंगे गुब्बारे, टेबल पर सजा बड़ा केक, बच्चों की चहचहाहट — सबकुछ जैसे परियों की दुनिया का हिस्सा लगता था।
पर इस बार जब अदिति के जन्मदिन की बारी आई, तो न घर में कोई सजावट थी, न केक, न ही किसी को याद था कि आज उसका भी जन्मदिन है।
शाम तक उसने चुपचाप घर के सारे काम निपटाए, सबको खाना परोसा, और खुद को भी एक कप चाय बनाई। फिर रसोई के कोने में बैठकर पुराने फोटो एल्बम के पन्ने पलटने लगी।
एक तस्वीर में वह मुस्कुरा रही थी — अपने बचपन के जन्मदिन पर, केक काटते हुए।
उसने चुपचाप उठकर फ्रिज से कुछ मैदा और दूध निकाला। रात के सन्नाटे में उसने अपना पहला केक खुद के लिए बनाया — साधारण, बिना क्रीम वाला।
जब सब सो गए, वह बालकनी में बैठकर वह केक खा रही थी — हर कौर में खुद के लिए थोड़ी मिठास, थोड़ी परवाह मिल रही थी।
उसने मन ही मन कहा — “हैप्पी बर्थडे अदिति। तुम्हारा होना भी खास है।”
उस रात पहली बार उसने खुद को जन्मदिन का उपहार दिया — आत्म-स्मरण।
32. गुमनाम विद्रोह
रेखा के हाथों में कलम थी, लेकिन आवाज़ नहीं। वह एक शिक्षिका थी, लेकिन जो बात वह कक्षा में बच्चों को निडर होकर सिखाती थी, वो अपने ही जीवन में कह नहीं पाती थी।
पति का व्यवहार रूखा था, सास का ताना रोज़ का था, और स्कूल में भी वह वरिष्ठों के तंज का शिकार होती। लेकिन वह सब सुनकर चुप रह जाती।
एक दिन स्कूल की एक छात्रा ने चुपचाप उसके हाथ में एक पुर्जा रखा — “मैम, आप सबसे हिम्मती हो। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ।”
रेखा ने वह पुर्जा रात भर तकिए के नीचे रखा, जैसे किसी युद्ध के लिए ओढ़ा गया कवच हो।
अगले दिन स्टाफ मीटिंग में जब फिर से उसे टोंका गया, तो पहली बार उसने कहा — “मैं सिर्फ काम करती हूँ, खुशामद नहीं।”
सन्नाटा छा गया। रेखा खुद भी चौंकी, पर भीतर एक क्रांति की चिंगारी महसूस हुई।
उसने समझा — विद्रोह का अर्थ हमेशा नारे लगाना नहीं होता, कभी-कभी सिर्फ ‘न’ कहना ही काफी होता है।
उस दिन से रेखा की चुप्पी में भी आवाज़ थी, और उसकी चुप्पी का हर शब्द, एक गुमनाम विद्रोह था।
33. किचन टाइमर
रमा के जीवन की घड़ी रसोई के किचन टाइमर से चलती थी। सब्ज़ी पकने के टाइम, चाय चढ़ाने का टाइम, बच्चों को दूध देने का टाइम — सब कुछ उस छोटे से टाइमर की टक-टक से बंधा था।
कभी वह सोचती — क्या कोई ऐसा टाइमर है जो बता सके, कब वो खुद के लिए जिए? कब वो सिर्फ रमा हो, माँ, पत्नी, बहू नहीं?
एक दोपहर रसोई में काम करते-करते अचानक टाइमर की बैटरी खत्म हो गई। टक-टक रुक गई। पहले तो वह घबरा गई — “अब कैसे पता चलेगा क्या कब करना है?”
फिर उसने सोचा — “क्या मैं इतनी भी नहीं कि बिना मशीन के अपने दिन को महसूस कर सकूं?”
उसने पहली बार टाइमर के बिना खाना बनाया — बिना घड़ी की सुइयों के डर के, बिना जल्दबाज़ी के। उसने बैठकर गरम रोटी खाई, बिना सबको परोसने की चिंता किए।
उस दिन रमा ने जाना — समय को पकड़ने के बजाय, उसे जीना ज़रूरी है।
अब भी टाइमर चलता है, पर अब रमा की ज़िंदगी उसकी टक-टक से नहीं चलती। अब वह तय करती है, कब और कैसे जिए।
34. लौटती चिट्ठियाँ
पूनम हर महीने माँ को चिट्ठी लिखती थी। मोबाइल युग में भी उसने वह पुरानी आदत नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जवाब नहीं आता था।
माँ की आँखें कमज़ोर हो गई थीं, हाथ काँपते थे। लेकिन पूनम को लगता था कि माँ अब भी उसका लिखा पढ़ती होंगी, महसूस करती होंगी।
एक बार उसने मज़ाक में लिखा — “माँ, अब तो ईमेल सीख लो।”
कुछ दिन बाद वही चिट्ठी डाकघर से ‘लौटी हुई’ आई — ‘पता नहीं मिला।’
उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कॉल किया तो पड़ोसी ने बताया — माँ को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
पूनम दौड़ी गई, और माँ के बिस्तर के पास बैठकर सारी पुरानी चिट्ठियाँ पढ़ने लगी। माँ की आँखों से आँसू बहते गए, होंठ हिलते गए, मानो सब याद कर रही हों।
माँ बोलीं — “तेरी चिट्ठियों से ही तो जीती रही बिटिया। जवाब भले न भेज पाई, पर हर शब्द पढ़ा था मैंने।”
अब पूनम हर चिट्ठी के साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजती है — ताकि माँ सिर्फ पढ़ें नहीं, सुने भी।
35. चुप्पियों का मेला
संध्या एक गांव के मेले में हर साल जाती थी — झूले, मिठाइयाँ, चूड़ियाँ। लेकिन इस साल वह अकेली गई। पति शहर गया था, बेटी ससुराल।
मेलों में भीड़ होती है, लेकिन कभी-कभी सबसे ज्यादा अकेलापन भी वहीं महसूस होता है।
संध्या चूड़ी की दुकान पर रुकी, मगर किसी ने पहनाने को हाथ नहीं बढ़ाया। झूले पर बैठी, पर बगल में कोई साथ हँसने वाला नहीं था।
वह मूक दर्शक बनकर सब देखती रही। तभी एक बूढ़ी महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा — “बेटी, अकेली हो? चलो, साथ चाय पीते हैं।”
संध्या ने पहली बार चुप्पी तोड़ी — “हाँ माँजी, चुप्पियों का मेला लग गया है आज मन में।”
वे दोनों चाय की गुमटी पर बैठीं, बिना ज़्यादा बोले चाय पीती रहीं।
उस दिन संध्या ने जाना — अकेलापन तब कम होता है जब कोई और भी अपनी चुप्पी से तुम्हारी चुप्पी को समझ सके।
अब वह हर साल मेले में उस बूढ़ी महिला को ढूंढती है — क्योंकि कभी-कभी सबसे खूबसूरत मेल वो होते हैं, जो शब्दों के बिना भी लगते हैं।
36. टूटी चूड़ियाँ
नीला रंग रमा की पसंदीदा चूड़ियों में से था। शादी के बाद जब वह पहली बार मायके से ससुराल आई थी, तो माँ ने एक कांच की नीली चूड़ियों का सेट उसे देते हुए कहा था — “इनमें तुम्हारा सारा प्यार बंद है। संभालकर रखना।”
रमा ने वर्षों तक उन्हें पहनकर रखा, हर त्योहार, हर विशेष दिन पर वह वही चूड़ियाँ पहनती। जब पति की बेरुखी, सास के ताने और बच्चों की उपेक्षा बढ़ने लगी, तब भी वे चूड़ियाँ उसकी कलाई पर बनी रहीं — जैसे आत्मसम्मान की आखिरी निशानी।
एक दिन झगड़े के दौरान पति ने उसका हाथ झटकते हुए कहा — “बस बहुत हो गया, अब नाटक मत करो।”
चूड़ियाँ ज़मीन पर गिरीं और टूट गईं।
रमा देर तक उन टुकड़ों को देखती रही। उनमें खुद का बिखराव नज़र आ रहा था। फिर उसने चुपचाप उन टुकड़ों को उठाया, उन्हें अख़बार में लपेटा और माँ की तस्वीर के नीचे रख दिया।
अगले दिन उसने स्टील की चूड़ियाँ खरीदीं। न रंग था, न आभा, पर वह जानती थी — अब कोई इन्हें आसानी से नहीं तोड़ पाएगा।
चूड़ियों के साथ रमा की आत्मनिर्भरता का नया अध्याय शुरू हुआ। वह जान गई थी — जब भावनाएँ टूटती हैं, तब आत्मबल की चूड़ियाँ पहननी पड़ती हैं।
37. सौंधी ख़ामोशी
मिट्टी की खुशबू बारिश के पहले कणों के साथ आती है, और विभा को ये खुशबू अपनी माँ की रसोई की याद दिला देती है। माँ जब गुड़ की चाय चढ़ाती थीं, तो पूरा घर सौंधी ख़ामोशी से भर जाता था — जैसे बिना बोले कोई गीत बज रहा हो।
शादी के बाद विभा एक फ्लैट में रहने लगी, जहाँ मिट्टी नहीं थी, बस कंक्रीट और नमी की गंध। बारिश भी वहाँ काँच से टकराकर आती थी, मिट्टी से नहीं।
एक दिन उसने बालकनी में कुछ गमले लगाए और एक छोटा सा तुलसी का पौधा बोया। पहली बारिश में वह भीगने बाहर आई, और मिट्टी की वही पुरानी सौंधी ख़ुशबू फिर से उसकी नाक में घुल गई।
वह आँखे बंद कर बैठ गई और माँ की खामोश मुस्कान याद आ गई।
उसने चाय बनाई, गुड़ वाली। पति ने पूछा — “आज कुछ खास?”
विभा मुस्कुराई — “हाँ, आज माँ आई थीं बारिश में।”
कुछ यादें शब्दों की मोहताज नहीं होतीं, वो सौंधी ख़ामोशी में भी जी उठती हैं।
38. गुमशुदा खिलौने
पायल जब माँ बनी, तो उसने अपने बेटे के लिए हर वो खिलौना खरीदा, जो वह अपने बचपन में नहीं पा सकी थी।
लेकिन एक खिलौना था, जो उसके दिल में चुभता रहा — एक लकड़ी का हाथी, जो उसे बहुत पसंद था और जो एक दिन पड़ोस की लड़की ले गई और कभी लौटाया नहीं।
बचपन में पायल ने किसी से शिकायत नहीं की, बस हर रात सोने से पहले खाली जगह को निहारती।
अब जब उसका बेटा वही लकड़ी का हाथी देखकर बोला — “माँ, ये बहुत प्यारा है!”, तो उसकी आंखों में बचपन लौट आया।
उसने बेटे को गोद में लेकर कहा — “अगर कभी कोई तुम्हारा खिलौना ले जाए, तो कहना — मुझे फर्क पड़ता है। क्योंकि चुप रहना सबसे लंबा नुकसान होता है।”
पायल ने जाना — कई गुमशुदा चीज़ें खिलौनों से ज़्यादा हमारे आत्मविश्वास को चुराती हैं। और उन्हें वापस पाना, खुद को वापस पाना है।
39. अधजली मोमबत्ती
नीरा रोज़ पूजा में एक मोमबत्ती जलाती थी — सफेद, पतली और सुगंधित। वो मानती थी कि जब तक उसकी लौ जलती है, घर में उम्मीद बाकी है।
एक दिन बेटी ने पूछा — “माँ, आप हर बार अधजली मोमबत्ती को क्यों रख लेती हो?”
नीरा मुस्कुराई — “क्योंकि इसमें अधूरी रोशनी बाकी है। जैसे हम सबमें होती है।”
वह अधजली मोमबत्तियाँ दराज़ में सहेजकर रखती। जब बिजली जाती, तो वही अधजली मोमबत्तियाँ काम आतीं — अंधेरे में टिमटिमाती, जैसे कह रही हों — ‘हम अब भी यहाँ हैं।’
एक दिन नीरा बीमार हो गई। बेटी ने वही दराज़ खोलकर अधजली मोमबत्ती जलाई, और माँ के सिरहाने बैठ गई। माँ ने आँखें खोलीं और धीमे से कहा — “रोशनी कभी पूरी नहीं होती, लेकिन उसे बचाए रखना ज़रूरी होता है।”
40. कुर्सी का कोना
सुधा के घर में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जो बरामदे में रखी रहती थी। उस पर कभी दादी बैठती थीं, फिर माँ, अब सुधा खुद।
वो कुर्सी उसकी अकेली जगह थी — चाय का पहला घूंट, किताब की पहली पंक्ति, और कभी-कभी आँसू की पहली बूँद वहीं गिरती।
परिवार में किसी को उस कोने से मतलब नहीं था, लेकिन सुधा जानती थी — वह कोना उसकी पहचान है।
एक दिन बहू ने कहा — “माँ, इस कुर्सी को हटा देते हैं, जगह घेरती है।”
सुधा चुप रही। रात को उसने वही कुर्सी बेटे के कमरे के बाहर रख दी और एक पर्ची उस पर चिपकाई — “कभी थक जाओ, तो यहाँ बैठ जाना। ये सिर्फ कुर्सी नहीं, सुकून है।”
सुबह बेटे ने माँ से कहा — “माँ, ये कुर्सी यहीं रहेगी। इसमें आपकी याद और हमारी ज़रूरत बसी है।”
कुछ कोने घर के नहीं, दिल के होते हैं — और कुछ कुर्सियाँ बस लकड़ी की नहीं होतीं, इतिहास की होती हैं।
प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,